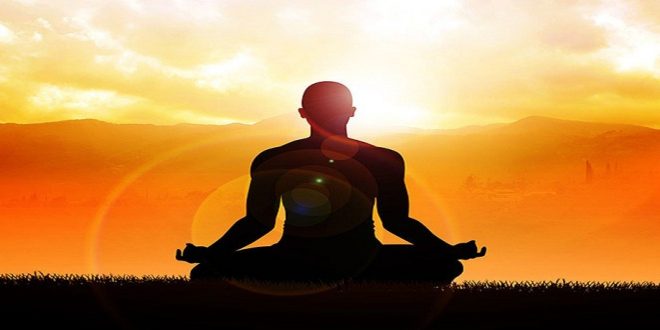आसन का अर्थ किसी तरह का शारीरिक अभ्यास नहीं है। इसका अर्थ ध्यान के लिए शरीर को स्थिरता से बिना हिलाए-डुलाए बैठना है। आशय सिर्फ बैठने की विधि से नहीं, उस स्थान और वातावरण से है, जहां ध्यान किया जाए। पातंजल योगदर्शन की मानें, तो शरीर को थकाने वाले अभ्यासों से, स्थिरता और सुविधा से बैठने पर ज्यादा आध्यात्मिक लाभ होता है।

इन निर्देशों को मानें तो योग साधना के लिए सिद्धासन, सर्वांगासन, पद्म्सन आदि पैरों को मोड़ने-तोड़ने के विधि-विशेष को नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस वातावरण का संकेत समझना चाहिए, जहां उपासना या ध्यान धारण किया जाना है। साधना में मन न लगने, जी ऊबने , चित्त के चंचल रहने की शिकायत साधकों को प्रायः रहती है। इसके आंतरिक कारणों के अलावा वातावरण का प्रभाव खासतौर पर रहता है।
जिस श्रद्धा-विश्वास से साधना की जानी चाहिए, उसका समावेश न हुआ, तो साधन छुट-पुट कर्मकांडों के सहारे न हो सकेगा। कठ, श्वेताश्वतर, छांदोग्य आदि शंकराचार्य के भाष्य लिखे प्रमुख उपनिषदों स्वामी विवेकानंद के राजयोग, श्रीअरविंद के योग समन्वय और योगदर्शन के पातंजल सूत्रों पर हरिहरानंद आरण्यक, स्वामी ओमानंद, तीर्थ स्वामी सत्यानंद सरस्वती आदि की टीकाओं में आसनों का कहीं इतना विस्तार नहीं है कि वही योग की चर्चा मान ली जाए।
आठ अंगोेें में से एक बहिरंग साधन के रूप में उल्लेखित आसन का संबंध आसानी से और बिना हिले-डुले बैठने से ही है। वह सिर्फ पैरों का नहीं पूरे शरीर का होता है। कमर सीधी, आंखें अधखुली, चित्त शांत और शरीर की स्थिति स्थिर रहनी चाहिए। मात्र ध्यान करना हो, तो दोनों हाथ गोदी में रहना चाहिए। जप और पूजा पाठ के कर्मकांड करना हो, तो ठीक, वरना हाथों को स्थिर ही रखना चाहिए।
इस तरह स्थिर और सुविधा से बैठने का शरीर और मन पर असर पड़ता है। उत्तानपाद, मत्स्यासन, मयूरासन, शीर्षासन आदि चौरासी या कम ज्यादा संख्या में गिनाए जाने वाले आसन शारीरिक व्यायाम हैं। आरोग्य रक्षा की दृष्टि से इनका व्यायाम जैसा ही महत्त्व है। इन्हें आध्यात्मिक साधनाओं में शामिल नहीं किया जाता। साधना के लिए बैठने में सुखासन उपयुक्त है। इसे किसी भी साधना में बिना किसी संकोच के किया जा सकता है।
 Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal